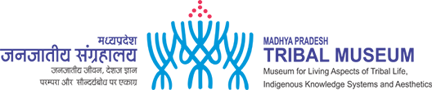1. यह संग्रहालय किसके लिये है? अर्थात् उसका संभावित दर्शक कौन है?
2. उस दर्शक का वर्तमान मानस क्या है? उसकी चिन्ताएँ क्या हैं? उसकी अभिरूचियाँ, आकांक्षाएँ अथवा स्वप्र क्या हैं? ....आदि।
3. संग्रहालय का अन्य तमाम सांस्कृतिक संस्थानों से इतर अपनी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? उसकी सार्थकता और उसका वैशिष्ट्य क्या होगा?
4. वह किन अर्थों में विभिन्न समुदायों के बीच सार्थक संवाद का एक नया सेतु निर्मित कर सकता है?
दर्शक वर्ग एक बहुत बड़ी और जटिल इकाई है, जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध, ग्रामीणजन, सभी वर्गों-समुदायों के स्त्री-पुरुष सम्मिलित हैं। उपरोक्त कोटियों में फिर अनेक विभेद हैं। मसलन-कुछ जिनका पहले से ही संस्कृति के प्रति एक राग है, पूर्व पीठिका है। कुछ जिनके लिये संस्कृति शब्द आज के समय में कोई मायने ही नहीं रखता। वह जीवन को अतीतोन्मुखी और इसीलिये विकास की विपरीत धारा में ले जाता है। तीसरी और संभवत: सबसे बड़ी कोटि उन लोगों की है, जो तमाम सांस्कृतिक प्रश्नों के प्रति पूरी तरह से उदासीन हैं। उन्होंने न इस बारे में सोचा है न सोचने की जरूरत ही जान पड़ी है।
संग्रहालय के लिये सभी संभावित दर्शक हैं और समान रूप से महत्त्व के हैं, क्योंकि संग्रहालय की सार्थकता उन्हीं से बड़ी से बड़ी संख्या में जुडऩे और संवाद कायम करने से ही है। जनजातीय संग्रहालय की राह एक अर्थ में दुधारी तलवार के मानिन्द हैं, क्योंकि एक ओर उसका मूल उद्देश्य आदिवासी जीवन दृष्टि को सांगोपांग समझना तथा प्रस्तुत करना है, तो दूसरी ओर उसे नागर समाज तक प्रेषित करना है, जिसने अपने लिये विकास अथवा जीवन को जीने की एक नितान्त भिन्न शैली को न केवल अपना लिया है, बल्कि उसे विकल्पहीन मान लिया है। इस संग्रहालय ने ऐसी ही जमीन तलाशी और तैयार की है, जहाँ समाज की यह दोनों विपरीत जान पड़ती धाराएँ परस्पर एक दूसरे की ओर उन्मुख होती हैं।
मोटे तौर पर आज की शहरी आधुनिक जीवन पद्धति को हम वैज्ञानिक विचार दृष्टि पर तथा आदिवासी जीवन पद्धति को मिथकीय दृष्टि पर आधारित मान सकते हैं। यदि किसी धरातल पर इन दोनों दृष्टियों के बीच संवाद होता आया है, तब वही इस संग्रहालय की वीथिकाओं में दृश्यमान आदिवासी जीवन बोध और आधुनिक जीवन बोध के बीच संवाद की पीठिका बना है।
गौर से देखें तो वैज्ञानिक चिन्तन तथा मिथकीय दृष्टि दोनों जिस मूल प्रश्न से सर्वप्रथम जुड़ते हैं, वह प्रश्न है- सृष्टि कैसे हुई? और यदि इस कैसे का विस्तार करें तो यह जो हमें घेरे है- हमारा पर्यावरण या उसके आगे आकाश या शून्य कैसे बने? समूचा मानव और मानवेत्तर समाज कैसे बना? और फिर जो ये प्रश्न खड़े कर रहा है, वह 'मैं' कौन है? कहाँ है?
ये चार ऐसे मूल प्रश्न हैं, जिनके उत्तर देने का प्रयास मिथकों तथा विज्ञान दोनों ने किया है। इस बात की पहचान बहुत आवश्यक है कि विज्ञान और मिथक दोनों का आरम्भ इस समान प्रश्न-भूमि से ही हुआ था, यद्यपि इसकी भी ठीक-ठीक पहचान उतनी ही आवश्यक है कि कहाँ जाकर इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। 18वीं-19वीं शदी के आते-आते विज्ञान की प्रगति ऐसी हुई कि जिसके चलते उल्लेखित चार प्रश्नों में से अन्तिम का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और सृष्टि की धुरी अपनी जगह से हट गई। अब मनुष्य स्वयं सृष्टि का केन्द्र बन गया।
'मैं' कौन हूँ? कहाँ हूँ? यह प्रश्न केवल मनुष्य पूछता है। वह स्वयं को इनका क्या उत्तर देता है उसी से यह तय होता है कि उसका सृष्टि से, समाज से और स्वयं अपने से क्या नाता होगा। हर संस्कृति की एक सृष्टि कथा होती है और उसी से वह सांस्कृतिक दृष्टि बनती है, जिससे संस्कृति अपने को देखती-पहचानती है। विज्ञान ने भी एक सृष्टि कथा प्रस्तुत की है, जिसमें वह प्रयोगों द्वारा बदलाव की संभावना को खुला रखता है। विज्ञान जहाँ 'ऐतिहासिक' भविष्य के प्रति खुला है, वहीं मिथकीय चेतना की खोज सतत् रूप से सनातन तत्त्व की रहती है। मिथकीय घटना क्रम वह सनातन घटना है, जिसमें हम मानव नियति के साथ हर नए युग में नए रूप से जुड़ सकते हैं। इसीलिये मिथक और पुराण ऊर्जा के स्त्रोत हैं, क्योंकि उनके सहारे हम अपने होने को, अपनी अवस्थिति को समग्र रूप से जान सकते हैं।
मिथक के कालबोध में परिवर्तन तो अवश्य है, किन्तु परिवर्तन का मूल्य 'आगे बढऩे की होड़' में नहीं है- सच पूछो तो वह कोई मूल्य ही नहीं है। वह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है- मृत्यु और पुनर्जीवन का एक चक्राकार, अनवरत सिलसिला जिसमें अतीत और भविष्य दोनों ही चिरंतन वर्तमान में गुंफित हैं। उदाहरण के लिये गोंड, भील अथवा बैगा सृष्टि मिथकों को लें : इन सभी में सृष्टि का कोई ऐसा आरम्भ बिन्दु नहीं है, जब कुछ भी नहीं था। मिथक के भीतर बड़ादेव को यह स्मृति है कि धरती जो अभी कहीं नज़र नहीं आ रही, वह कुछ समय पूर्व तक पानी पर थी। बड़ादेव सृष्टि करें, इसके पूर्व ही जलचर-साँप, केकड़ा, केंचुआ आदि पहले से विद्यमान हैं और उन्हें धरती का पता-ठिकाना भी मालूम है। भील मिथक में जब धरती पर भारी उलट-पलट हुई और सब कुछ जल प्लावित हो गया, तब भी पावागढ़ पर्वत नहीं डूबा और उसने जीवन के बीज को बचा लिया। इस तरह न संपूर्ण मृत्यु है या पूरी तरह से मिट जाना है-न कोई ऐसा आरंभ बिन्दु कि जिसके पहले कुछ भी नहीं था। शून्य भी यहाँ निरा शून्य कहाँ है? निराकार में ही समस्त रूप विद्यमान हैं। नृतत्वशास्त्री लेवी-स्ट्रॉस के शब्दों में 'जहाँ प्रागैतिहासिक समाज इतिहास के तत्त्वों से घिरे होने के बावजूद उससे उदासीन और अछूता रहने का प्रयत्न करता है, वहाँ आधुनिक समाज इतिहास को अपने भीतर समाहित कर लेता है और उसे (इतिहास को) अपने विकास का प्रेरणा स्त्रोत मान लेता है।
विज्ञान की अद्यतन सृष्टि कथा में सृष्टि के आरंभ बिन्दु की अवधारणा है। साथ ही विज्ञान दिग्विस्तार की एक सीमा भी मानता है, जिसके परे कुछ नहीं है। वहाँ से प्रकाश किरणें भी लौट आती हैं, अत: काल की पहुँच भी वहीं तक है। मिथक बोध या कला बोध को तो इससे खास आपत्ति नहीं होगी, किन्तु स्वयं विज्ञान के लिये इसमें एक जबरदस्त पेंच है। समस्या यह उठती है कि ऐतिहासिक, एकरेखीय और एक दिगुन्मुख काल का अन्त कैसे हो सकता है? जब वैज्ञानिक कहता है कि एक सीमा से दिक् भी मुड़कर लौट आता है, तब ऐसा कहने का ठीक-ठीक अर्थ क्या हुआ, इसे लेकर वैज्ञानिक विचार असमंजस में पड़ जाता है। विज्ञान और मिथकीय सृष्टि कथाएँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, किन्तु सृष्टि का वर्तमान विस्तार कैसा है-पदार्थ, ऊर्जा, दिक् और काल के आपसी संबंध क्या हैं! यह समझाते हुए वैज्ञानिक आज यह देखकर चकित रह जाता है कि जिस शब्दावली का प्रयोग वह कर रहा है, वह उस शब्दावली से बहुत भिन्न नहीं हैं, जिसका उपयोग मिथक रचने वालों ने किया है।
सवाल वैज्ञानिक अथवा मिथकीय दृष्टि के पक्ष-विपक्ष में खड़े हो जाने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या मिथकीय चिन्तन की राह सचमुच चिन्तन की एक संभावित दूसरी राह है? क्या रूपकाश्रयी चिन्तन (एनालॉजिकल) वैज्ञानिक चिन्तन (लॉजिकल) का समानान्तर और पूरक हो सकता है? वैज्ञानिक और मिथकीय चेतना के बीच एक और धरातल है, जिसकी संगति उपरोक्त दोनों से है, किन्तु साथ ही जिसकी अपनी स्वतंत्र दृष्टि और जगत पसारा भी है- कलाबोध अथवा एस्थेटिक। ललित, नान्दतिक, एस्थेटिक के प्रश्न भी अन्तत: उन चार मूल सवालों से जुड़ जाते हंै। क्योंकि रूप सौष्ठव के विचार में ये सारे प्रश्न जुड़ते हैं कि आकाश, शून्य, दिक् अथवा स्पेस क्या है? दिक् काल क्या है? दिक् चक्र कहाँ है? उसकी धुरी कहाँ है? सृष्टि की धुरी और उसे जानने की इच्छा रखने वाली चेतना की धुरी में क्या संबंध है? अनुलम्ब और ऊध्र्वाधर क्या है? प्रकाश और अन्धकार क्या हैं? आकाश क्या भीतरी और बाहरी भी होता है? प्रकाश के साथ ऊपर और अन्धकार के साथ 'नीचे क्यों जुड़ा है...आदि?
कलाबोध की स्थिति मध्यगामी है- उसे न वैज्ञानिक प्रयोगधर्मिता से परहेज़ है न सनातन तत्त्वों से। चेतना की उपज होते हुए भी कला अवचेतन की जड़ों में अपनी सार्थकता खोजती है। वह विज्ञान के उन सब 'युक्तिसंगत', तार्किक और बौद्धिक अंधविश्वासों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, जो आधुनिक सभ्यता की आधार शिला हैं। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज के समय में सार्थक कला कमोबेश वही भूमिका अदा करती है, जो आदिकाल में मिथक चेतना करती थी- मानव जीवन के असंगत, अराजक और अर्थहीन क्रियाकलाओं को उसके कालातीत मर्म के चौखटे में संयोजित करना।
किन्तु मिथक उस अर्थ में मनुष्य द्वारा नहीं सिरजे गये, जिस अर्थ में मनुष्य कला का सृजन करता है। मिथक मनुष्य की सर्जना न होकर मनुष्य की अज्ञात, अनाम, सामूहिक चेतना का अंग है। इसे यूँ कह सकते हंै कि कला में जो सचेत रूप से प्राप्त किया जाता है, वह मिथक के परिवेश में पहले से ही नैसर्गिक रूप से मौजूद रहता है। लेखक/चिंतक निर्मल वर्मा के शब्दों में 'कला अपने सृजन के उदात्ततम क्षणों में मिथक होने का स्वप्र देखती है, एक ऐसा स्वप्र जिसमें व्यक्ति और समूह का भेद मिट जाये।
आधुनिक शहरी मनुष्य की त्रासदी दुहरी है, क्योंकि वह पहले प्रकृति से और फिर समाज से अलग हुआ। इन दोनों अलगावों ने मनुष्य के भीतर एक भयानक अकेलेपन को जन्म दिया है। दूसरी ओर आदिवासी समाज का प्रकृति अथवा पर्यावरण से संबंध पूरी तरह से खंडित नहीं हुआ है। यह खंडन उन पर बाहरी परिस्थितियों द्वारा आरोपित है, यानी प्रकृति से विच्छेद की स्थिति उनकी स्वयं स्वीकारी हुई नहीं है। अलावा इसके आदिवासी मनुष्य अभी भी अपने समूह से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसका निजी अनुभव एक सामुहिक चेतना का ही अंग है। उसकी दूसरों के और दूसरों की उसके अनुभव में साझेदारी रहती है।
मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश के आदिवासी जनों ने दीर्घाओं को आकार दिया। उनके द्वारा तैयार किये गये रूपाकारों में आदिवासी जीवनदृष्टि और कलाबोध से जुड़ी कई विलक्षण बातें नए सिरे से उद्घाटित हुई हैं। मसलन-इन कामों में प्राय: चेतन-अवचेतन, मनुष्य और प्रकृति, आत्मा और देह के कृत्रिम विभेद नहीं हैं। इसी के चलते इन कलारूपों में जहाँ एक ओर आदि घटना की उत्कट कौंध और ऊर्जा है तो दूसरी ओर सामुदायिकता की गरमाहट और आश्वासन भी है।
किन्तु शहरी और आदिवासी समाज की जीवन दृष्टियों के बीच सार्थक संवाद कायम कर पाने की चुनौती को भाषा में समझ लेने के बावजूद उसे भौतिक, मूर्ति रूप देना बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियाँ नए सिरे से खड़ी करता है। उदाहरण के लिये सबसे पहले तो यही कि आदिवासी जीवन के केन्द्र में भौतिक समृद्धि या कहें भौतिकता नहीं है- इसलिये उनका जीवन भौतिक वस्तुओं से यथासंभव दूरी बनाये हुए है। संग्रहालय के लिये विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों से भौतिक संग्रह करने के दौरान इस तथ्य को मार्मिकता से अनुभव किया गया। और यदि कुछ भौतिक वस्तुएँ हैं भी तो वे शहरी भोक्ता समाज को प्राय: गौण जान पड़ेंगी।
वहीं दूसरी ओर इन 'सरल', 'साधारण' और न मालूम-सी जान पडऩे वाली वस्तुओं के अभिप्राय, कम से कम उस समाज के लिये बहुत गहरे और व्यापक हैं। हमें जो साधारण, अनगढ़, रास्ते के किनारे रखा 'पत्थर' जान पड़ेगा, उसमें न जाने कैसी-कैसी विपदाओं को छेंकने और उनके कुप्रभावों को नष्ट कर देने की शक्ति है। इस जीवन दृष्टि की लय में तमाम भौतिक-अभौतिक पक्ष परस्पर इस कदर गुँथे हुए हैं कि 'सूपा'-रसोई घर की वस्तु (हाउस होल्ड) भी है, संस्कार से-अनुष्ठान से, कलाबोध से भी इसका नाता है और अलावा इसके यह किसी समुदाय विशेष के लिये आर्थिक कमाई का भी साधन है। एक 'सूपे' से जुड़ी बाँसिन कन्या (बाँस) की जन्मकथा है, जिसमें अपने छ: भाईयों द्वारा मारी गई बहन अपने सातवें भाई के त्याग और प्रेम से बल पाकर घने जंगल में बाँस के रूप में दुबारा जन्म लेती है, और मानव जाति के लिये जन्म से मृत्यु तक के तमाम संस्कारों के लिये अनिवार्य बन जाती है। इन समाजों में बच्चे के जन्म लेने पर उसे माँ की गोद से पहले धान-कोदो से भरे सूपे में लिटाया जाता है। सूपे से जुड़ी ऐसी कितनी ही अन्य बातें और गीत हैं। अब दिक्कत यह खड़ी होती है कि आधुनिक वास्तु शैली की इस गगन चुंबी दीवारों वाली दीर्घा में इस अंकिचन, सरल, साधारण वस्तु को कैसे दिखाया जाए कि वह अपनी समस्त संभावनाओं और अर्थ के विस्तार में दर्शकों के लिये आलोकित हो सके?
लगभग यही बात उनके 'कलाबोध' उनके 'देवलोक' आदि पर भी लागू होती है। अव्यक्त-सी अभिव्यक्ति, जो जितना कहती है, उससे कहीं अधिक को अपने भीतर छुपाए रखती है। आदिवासी कलाबोध जैसे न दिखने की कला में निहित है।
इसीलिये यह तय किया कि मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय आदिवासी जीवन की अन्तर्चेतना को उसकी समग्रता में ही समझने और अभिव्यक्त करने की कोशिश करेगा। आदिवासी बल्कि भारतीय लोक चेतना के लिये प्रकृति के जड़ व चेतन तत्त्वों में कोई गहरा भेद नहीं है। सभी कुछ एक ही शक्ति से आविष्ट और अनुप्राणित है और इसीलिये गिरि-गह्वर, नदी-नाले, वृक्ष और दूब सब पूजनीय हैं। यह बात शिद्दत से महसूस हुई कि उपरोक्त बात का एहसास दीर्घा की पराई तथा कृत्रिम भूमि पर करवाने के लिये किसी न किसी उपाय से उस पर्यावरण और परिवेश को रचना होगा, जिसमें जंगल का उसके धूप-छाँही उजाले, उसके बीहड़पन का, उसकी ध्वनियों का एक सघन एहसास होता हो। संग्रहालय का लक्ष्य आदिवासी मिथकीय चेतना व कलाबोध के सार तत्त्व तक पहुँचना था और इसी को ध्यान में रखते हुए इन दीर्घाओं का आकल्पन किया गया है। कुछेक छायाचित्रों अथवा वस्तुओंं को दीवार पर मढ़कर या काँच के शोकेसों में सजाकर रखने का उपाय कारगर नहीं जान पड़ा। उसमें कृत्रिमता अधिक महसूस होती है, अलावा इसके उस तरह के आकल्पन में अभिव्यक्ति आधी-अधूरी और लक्ष्य से कोसों दूर रहती है। इसीलिये मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की दीर्घाओं में आदिवासी मिथकीय अन्तर्दृष्टि और कलाबोध को पकडऩे के लिये ऐसे उपाय किये गये हैं, जो अपने नवाचार के कारण कृत्रिम जान पड़ सकते हैं, पर वास्तव में वे इसी कृत्रिमता से भरसक मुक्ति पाने की उत्कंठा से जन्में हैं।
आधुनिक इमारत के भीतर आदिवासी जीवन दृष्टि को पकडऩे की चेष्टा अपने आपमें ही विरोधाभासपूर्ण है। यदि सच्चे अर्थों में हमें उस जीवन पद्धति और चिन्तन को जानना है, तो हमें उनके बीच, उनके परिवेश में जाना होगा। किन्तु जैसा कि शुरुवात में ही कहा गया, संग्रहालय का दायित्व तथा ध्येय शहरी और आदिवासी दोनों समाजों के प्रति और दोनों के बीच परस्पर संवाद की पृष्ठभूमि तैयार करना है। इसी कारण इन दीर्घाओं में जहाँ एक ओर प्राकृतिक उपादानों मसलन पुआल, पत्ते, पत्थर, मिट्टी, बाँस, लकड़ी, लोहा, सूखे वृक्षों-टहनियों आदि का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक औजारों, तकनीक, दृश्य-श्रव्य माध्यमों, प्रकाश संयोजन आदि का भी इस्तेमाल भविष्य में भी किया जायेगा। हर दीर्घा में प्रकाश संयोजन दिन के किसी प्रहर को ध्यान में रखते हुए करने का विचार है-मसलन जीवन शैली को अभिव्यक्त करती द्वितीय दीर्घा में सूर्योदय और भोर का उजाला होगा, जो किसी घर के छप्पर अथवा किसी घर के आँगन को आलोकित करेगा। उसी प्रकार देवलोक दीर्घा को दर्शक चाँदनी रात के निस्तब्ध उजाले में देखेंगे। ऐसे प्रकाश संयोजन के पीछे परिवेश को अधिक सजीव रूप में खड़ा करना, अनुभूति को सघन बनाना और दीर्घा में प्रदर्शित वस्तुओं (प्रादर्शों) की सतह के खुरदुरे-मुलायम, छिद्रित-ठोस एहसास, उनके नुकीले उभार और गोलाइयों को शिद्दत से महसूस कराना है। प्रदर्शनी को बहुआयामी, ज्ञानवद्र्धक चित्ताकर्षक तथा देशज ज्ञान से भरपूर किन्तु साथ ही दिलचस्प बनाये बगैर आज के इस तेज़ रफ्तार समय में दर्शकों को संग्रहालय की ओर मोडऩा संभव नहीं हो पाएगा।
संग्रहालय यह मानकर चल रहा है कि मिथकीय चेतना परिवर्तनशील है तथा हर काल में वह अपने को नवीन करती चलती है। हर आदिवासी अनुष्ठान दरसल उन आदिकालिक मिथकीय घटनाओं का अनुकरण या अभिनय न होकर उनका पुनर्घटन है। इस पुनर्जन्म रूपी नवीकरण में ही उसे नए अर्थ, नए रूपाकार मिलते हैं, जिसे हम सर्जनात्मक अभिव्यक्ति और इसलिये उसे स्वतंत्रता से जोड़कर आधुनिक समाज के पक्ष में मूल्य का दर्जा देते हैं, उसी सृजन की संभावनाओं के कपाट आदिवासी और लोक समाजों के लिये बंद कर देते हैं। कला में अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य की बात करते अचानक आदिवासी कलाबोध की बात तक आते-आते हम सीमा सुरक्षा चौकियाँ खोल बैठते हैं। हालांकि अब ये दुराग्रह बहुत हद तक टूटे हैं। नतीजतन, पिछले वर्षों में आदिवासी तथा लोक समाजों की कला और ज्ञान के क्षेत्र में उपस्थिति कई गुना बढ़ी है और इसके मूल्यांकन की प्रणालियों पर भी नए सिरे से विचार किया जा रहा है। शिक्षा के उच्चतम राष्ट्रीय संस्थानों में देशज ज्ञान और कला पद्धतियों मसलन लौह प्रगलन, वस्त्र रंगाई-छपाई आदि के प्रदर्शन के लिये अगरिया, पनिका, छीपा आदि समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के अनेक आदिवासी व लोक कलाकारों ने कला जगत में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है और अपने समुदाय की अस्मिता को नए सिरे से परिभाषित किया है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में काम किया गया है और उसकी जीवन्तता को अभिव्यक्त करने के लिए जारी भी रहेगा, जिनकी चाक्षुक अभिव्यक्ति आप दीर्घाओं और संपूर्ण परिसर में देखेंगे।
मध्यप्रदेश की विशिष्टता को स्थापित करने तथा उसकी बहुरंगी, बहुआयामी संस्कृति को बेहतर रूप से समझने और दर्शाने का कार्य दीर्घा क्रमांक-एक...
आगे पढेंदीर्घा-एक से दो में प्रवेश करने के लिए जिस गलियारे से गुजर कर जाना होता है, वहाँ एक विशालकाय अनाज रखने की कोठी बनाई गई है।...
आगे पढेंकलाबोध दीर्घा में हमने जीवन चक्र से जुड़े संस्कारों तथा ऋतु चक्र से जुड़े गीत-पर्वों-मिथकों, अनुष्ठानों को समेटने का उद्देश्य रखा है।...
आगे पढेंसंकेतों, प्रतीकों की जिस आशुलिपि में इस आदिवासी समुदाय ने अपने देवलोक के वितान को लिखा है, उसकी व्यापकता दिक्-काल की अनंत-असीम की ...
आगे पढेंअतिथि राज्य की आदिवासी संस्कृति को दर्शाती दीर्घा में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के जीवन को प्रस्तुत किया जा रहा है।...
आगे पढेंजीवन की भोर बेला यानी बचपन और उसके खेलों पर आधारित प्रदर्शनी इस दीर्घा में लगायी गई है। आदिवासी समुदायों में भौतिक वस्तुएँ नहीं के बराबर हैं...
आगे पढें